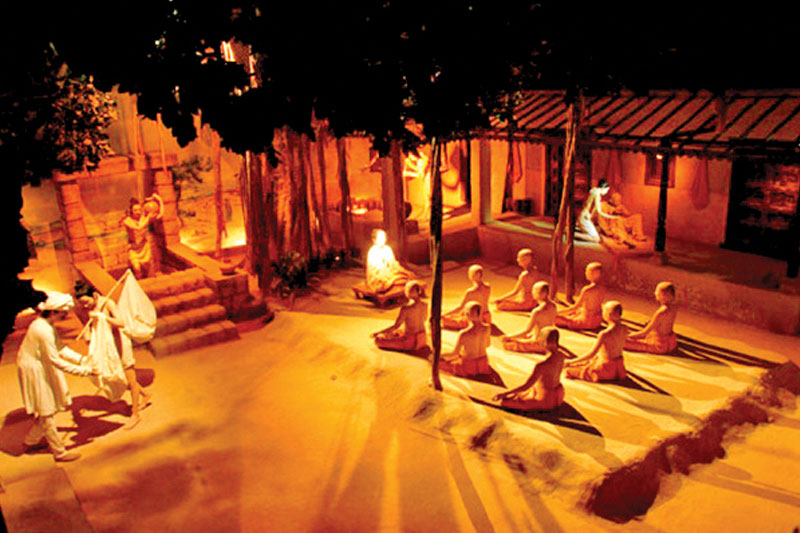
ÓżĢÓż┐ÓżĖÓźĆ Óż©Óźć Óż¢ÓźéÓż¼ ÓżĢÓż╣ÓżŠ Óż╣Óźł, 'ÓżĖÓżŠÓż«ÓżŠÓż©ÓźŹÓż» ÓżöÓż░ ÓżĖÓż░ÓźŹÓżĄÓźŗÓżżÓźŹÓżżÓż« ÓżČÓż┐ÓżĢÓźŹÓżĘÓżĢ Óż«ÓźćÓżé ÓżģÓżéÓżżÓż░ ÓżĖÓż┐Óż░ÓźŹÓż½ ÓżÅÓżĢ Óż¬ÓźŹÓż░ÓźćÓż░ÓżŻÓżŠ' ÓżĢÓżŠ Óż╣ÓźĆ Óż╣Óźł ÓżöÓż░ Óż»Óż╣ ÓżģÓżĢÓźŹÓżĘÓż░ÓżČÓżā ÓżĖÓżżÓźŹÓż» ÓżŁÓźĆ Óż╣ÓźłÓźż Óż£Óż╣ÓżŠÓżü ÓżÅÓżĢ ÓżĖÓżŠÓż«ÓżŠÓż©ÓźŹÓż» ÓżģÓż¦ÓźŹÓż»ÓżŠÓż¬ÓżĢ ÓżĖÓż┐Óż░ÓźŹÓż½ Óż£ÓżŠÓż©ÓżĢÓżŠÓż░Óż┐Óż»ÓźŗÓżé ÓżĢÓźŗ Óż¼ÓżŠÓżüÓżÜÓżżÓżŠ Óż╣Óźł; ÓżĄÓż╣ÓźĆÓżé ÓżÅÓżĢ ÓżĖÓż░ÓźŹÓżĄÓźŗÓżżÓźŹÓżżÓż« ÓżģÓż¦ÓźŹÓż»ÓżŠÓż¬ÓżĢ ÓżøÓżŠÓżżÓźŹÓż░ ÓżĢÓźĆ Óż£Óż┐Óż£ÓźŹÓż×ÓżŠÓżĖÓżŠ ÓżĢÓźŗ Óż¬ÓźŹÓż░ÓźćÓż░ÓżŻÓżŠ Óż░ÓźéÓż¬ÓźĆ Óż¬ÓżéÓż¢ Óż▓ÓżŚÓżŠÓżĢÓż░ Óż£ÓźŹÓż×ÓżŠÓż© ÓżĢÓźć ÓżģÓżĖÓźĆÓż« ÓżåÓżĢÓżŠÓżČ Óż«ÓźćÓżé ÓżēÓź£Óż©ÓżŠ ÓżĖÓż┐Óż¢ÓżŠÓżżÓżŠ Óż╣ÓźłÓźż ÓżåÓżćÓżÅ, ÓżćÓżĖ Óż▓ÓźćÓż¢ ÓżĢÓźć Óż«ÓżŠÓż¦ÓźŹÓż»Óż« ÓżĖÓźć ÓżĄÓźłÓż”Óż┐ÓżĢ ÓżåÓżÜÓżŠÓż░ÓźŹÓż»ÓźŗÓżé ÓżĢÓźć ÓżÉÓżĖÓźć Óż╣ÓźĆ ÓżĢÓżł Óż«ÓźéÓż▓ÓżŁÓźéÓżż ÓżŚÓźüÓżŻÓźŗÓżé ÓżĢÓźŗ ÓżåÓż£ ÓżĢÓźć Óż¬Óż░Óż┐Óż¬ÓźćÓżĢÓźŹÓżĘÓźŹÓż» Óż«ÓźćÓżé ÓżĖÓż«ÓżØÓż©Óźć ÓżĢÓżŠ Óż¬ÓźŹÓż░Óż»ÓżŠÓżĖ ÓżĢÓż░ÓżżÓźć Óż╣ÓźłÓżéÓźż
ÓżģÓżźÓż░ÓźŹÓżĄÓżĄÓźćÓż” ÓżĢÓżŠ ÓżåÓż░Óż«ÓźŹÓżŁÓż┐ÓżĢ ÓżČÓźŹÓż▓ÓźŗÓżĢ ÓżĖÓż«Óż» ÓżĢÓźć ÓżČÓż┐ÓżĢÓźŹÓżĘÓżĢÓźŗÓżé ÓżĢÓźĆ ÓżĄÓż┐ÓżČÓż┐ÓżĘÓźŹÓż¤ÓżżÓżŠÓżōÓżé ÓżĢÓżŠ Óż¼Óż¢ÓźéÓż¼ÓźĆ ÓżÜÓż┐ÓżżÓźŹÓż░ÓżŻ ÓżĢÓż░ÓżżÓżŠ Óż╣Óźł-
Óż¬ÓźüÓż©Óż░ÓźćÓż╣Óż┐ ÓżĄÓżŠÓżÜÓżĖÓźŹÓż¬ÓżżÓźć Óż”ÓźćÓżĄÓźćÓż© Óż«Óż©ÓżĖÓżŠ ÓżĖÓż╣Óźż
ÓżĄÓżĖÓźŗÓżĘÓźŹÓż»ÓżżÓźćÓż©Óż┐ Óż░Óż«Óż» Óż«Óż»ÓźŹÓż»ÓźćÓżĄÓżŠÓżĖÓźŹÓżżÓźü Óż«Óż»Óż┐ ÓżČÓźŹÓż░ÓźüÓżżÓż«ÓźŹÓźżÓźż
-ÓżģÓżźÓż░ÓźŹÓżĄÓżĄÓźćÓż” ( 1/1/2)
ÓżćÓżĖÓżĢÓżŠ ÓżĖÓż░Óż▓ÓżŠÓż░ÓźŹÓżź Óż╣ÓźüÓżå, 'Óż╣Óźć ÓżĄÓżŠÓżŻÓźĆ ÓżĢÓźć Óż¬ÓżżÓż┐! Óż”ÓźćÓżĄ-Óż«Óż© ÓżĢÓźć ÓżĖÓżŠÓżź Óż½Óż┐Óż░ ÓżåÓżćÓżÅ, ÓżĄÓżĖÓźü ÓżĢÓźć Óż¬ÓżżÓż┐! Óż©Óż┐Óż░ÓżéÓżżÓż░ Óż░Óż«ÓżŻ ÓżĢÓż░ÓżŠÓżćÓżÅÓźż Óż«ÓźüÓżØÓż«ÓźćÓżé ÓżĖÓźüÓż©ÓżŠ Óż╣ÓźüÓżå Óż«ÓźüÓżØÓż«ÓźćÓżé Óż╣ÓźĆ Óż░Óż╣ Óż£ÓżŠÓżÅÓźż'
ÓżŚÓźīÓż░ ÓżĖÓźć Óż¬ÓźØÓźćÓżé, ÓżżÓźŗ ÓżćÓżĖ Óż«ÓżéÓżżÓźŹÓż░ Óż«ÓźćÓżé ÓżČÓż┐ÓżĢÓźŹÓżĘÓżĢ ÓżĢÓźĆ ÓżÜÓżŠÓż░ ÓżĄÓż┐ÓżČÓż┐ÓżĘÓźŹÓż¤ÓżżÓżŠÓżōÓżé Óż¬Óż░ Óż¬ÓźŹÓż░ÓżĢÓżŠÓżČ ÓżĪÓżŠÓż▓ÓżŠ ÓżŚÓż»ÓżŠ Óż╣ÓźłÓźż Óż¬Óż╣Óż▓ÓźĆ, ÓżÅÓżĢ ÓżģÓż¦ÓźŹÓż»ÓżŠÓż¬ÓżĢ ÓżĢÓźŗ ÓżĄÓżŠÓżÜÓżĖÓźŹÓż¬ÓżżÓż┐ Óż╣ÓźŗÓż©ÓżŠ ÓżÜÓżŠÓż╣Óż┐ÓżÅÓźż Óż”ÓźéÓżĖÓż░ÓżŠ, ÓżČÓż┐ÓżĢÓźŹÓżĘÓżĢ ÓżĢÓźŗ Óż”ÓźćÓżĄ-Óż«Óż© ÓżĖÓźć Óż»ÓźüÓżĢÓźŹÓżż Óż╣ÓźŗÓż©ÓżŠ ÓżÜÓżŠÓż╣Óż┐ÓżÅÓźż ÓżżÓźĆÓżĖÓż░ÓżŠ, ÓżÅÓżĢ ÓżģÓż¦ÓźŹÓż»ÓżŠÓż¬ÓżĢ ÓżĢÓźŗ ÓżĄÓżĖÓźüÓż¬ÓżżÓż┐ ÓżŁÓźĆ Óż╣ÓźŗÓż©ÓżŠ ÓżÜÓżŠÓż╣Óż┐ÓżÅÓźż ÓżÜÓźīÓżźÓźĆ Óż»ÓźŗÓżŚÓźŹÓż»ÓżżÓżŠ Óż╣Óźł, ÓżģÓż¦ÓźŹÓż»ÓżŠÓż¬ÓżĢ ÓżĢÓżŠ Óż¬ÓżóÓżŠÓż╝Óż©Óźć ÓżĢÓżŠ ÓżóÓżéÓżŚ Óż░Óż«ÓżŻÓźĆÓż» ÓżöÓż░ Óż░ÓźŗÓżÜÓżĢ Óż╣ÓźŗÓźż ÓżåÓż”Óż░ÓźŹÓżČ ÓżåÓżÜÓżŠÓż░ÓźŹÓż»ÓźŗÓżé ÓżĢÓźć ÓżćÓż©ÓźŹÓż╣ÓźĆÓżé ÓżŚÓźüÓżŻÓźŗÓżé ÓżĢÓźŗ Óż¬ÓźéÓż░ÓźŹÓżŻÓżżÓżā ÓżĖÓż«ÓżØÓż©Óźć ÓżĢÓźć Óż▓Óż┐ÓżÅ, ÓżåÓżćÓżÅ ÓżćÓżĖ ÓżČÓźŹÓż▓ÓźŗÓżĢ ÓżĢÓżŠ Óż¼ÓżŠÓż░ÓźĆÓżĢÓźĆ ÓżĖÓźć ÓżĄÓż┐ÓżČÓźŹÓż▓ÓźćÓżĘÓżŻ ÓżĢÓż░ÓżżÓźć Óż╣ÓźłÓżéÓźż
ÓżČÓż┐ÓżĢÓźŹÓżĘÓżĢ 'ÓżĄÓżŠÓżÜÓżĖÓźŹÓż¬ÓżżÓż┐' Óż╣ÓźŗÓżé!
ÓżĄÓźłÓż”Óż┐ÓżĢ Óż”ÓźāÓżĘÓźŹÓż¤Óż┐ÓżĢÓźŗÓżŻ- ÓżĄÓźćÓż” Óż©Óźć ÓżČÓźŹÓż░ÓźćÓżĘÓźŹÓżĀ ÓżČÓż┐ÓżĢÓźŹÓżĘÓżĢ ÓżĢÓźĆ Óż¬Óż╣Óż▓ÓźĆ Óż»ÓźŗÓżŚÓźŹÓż»ÓżżÓżŠ- 'ÓżĄÓżŠÓżÜÓżĖÓźŹÓż¬ÓżżÓż┐' ÓżģÓż░ÓźŹÓżźÓżŠÓżżÓźŹ ÓżĄÓżŠÓżŻÓźĆ ÓżĢÓżŠ ÓżģÓż¦Óż┐Óż¬ÓżżÓż┐ Óż╣ÓźŗÓż©ÓżŠ ÓżĢÓż╣ÓżŠ Óż╣ÓźłÓźż ÓżÅÓżĢ ÓżÉÓżĖÓżŠ ÓżģÓż¦ÓźŹÓż»ÓżŠÓż¬ÓżĢ Óż£Óż┐ÓżĖÓżĢÓżŠ ÓżģÓż¬Óż©ÓźĆ Óż¼ÓźŗÓż▓ÓźĆ Óż¬Óż░ Óż¬ÓźéÓż░ÓźŹÓżŻÓżżÓż»ÓżŠ ÓżģÓż¦Óż┐ÓżĢÓżŠÓż░ Óż╣ÓźŗÓźż Óż£Óż┐ÓżĖÓżĢÓźĆ ÓżČÓż¼ÓźŹÓż”ÓźŗÓżé Óż¬Óż░ Óż«Óż£Óż¼ÓźéÓżż Óż¬ÓżĢÓź£ Óż╣Óźŗ ÓżöÓż░ ÓżĖÓżéÓżĄÓżŠÓż” ÓżČÓźłÓż▓ÓźĆ Óż¬ÓźŹÓż░Óż¢Óż░ Óż╣ÓźŗÓźż Óż«ÓżżÓż▓Óż¼ Óż£Óźŗ ÓżĄÓż╣ ÓżĢÓż╣Óż©ÓżŠ, ÓżĖÓż«ÓżØÓżŠÓż©ÓżŠ ÓżÜÓżŠÓż╣ÓżżÓżŠ Óż╣Óźŗ, ÓżēÓżĖÓźć ÓżĄÓż╣ ÓżøÓżŠÓżżÓźŹÓż░ÓźŗÓżé ÓżĢÓźć ÓżĖÓż«ÓżĢÓźŹÓżĘ Óż¼Óż¢ÓźéÓż¼ÓźĆ ÓżżÓźīÓż░ Óż¬Óż░ Óż░Óż¢ ÓżĖÓżĢÓźćÓźż ÓżĢÓźŹÓż»ÓźŗÓżéÓżĢÓż┐ ÓżģÓżŚÓż░ ÓżåÓż¬ ÓżÅÓżĢ ÓżĢÓźüÓżČÓż▓ Óż¬ÓźŹÓż░ÓżĄÓżĢÓźŹÓżżÓżŠ Óż©Óż╣ÓźĆÓżé Óż╣ÓźłÓżé, ÓżżÓźŗ ÓżåÓż¬ ÓżĄÓż┐Óż”ÓźŹÓż»ÓżŠÓż░ÓźŹÓżźÓż┐Óż»ÓźŗÓżé ÓżĢÓźć ÓżĖÓż«ÓżĢÓźŹÓżĘ ÓżģÓż¬Óż©Óźć ÓżĄÓż┐ÓżÜÓżŠÓż░ÓźŗÓżé ÓżĢÓźŗ ÓżĖÓż╣ÓźĆ ÓżżÓż░ÓźĆÓżĢÓźć ÓżĖÓźć ÓżĄÓźŹÓż»ÓżĢÓźŹÓżż Óż╣ÓźĆ Óż©Óż╣ÓźĆÓżé ÓżĢÓż░ Óż¬ÓżŠÓżÅÓżüÓżŚÓźćÓżéÓźż Óż£Óż┐ÓżĖ ÓżĄÓż┐ÓżĘÓż» Óż«ÓźćÓżé ÓżåÓż¬ ÓżēÓż©ÓźŹÓż╣ÓźćÓżé ÓżČÓż┐ÓżĢÓźŹÓżĘÓż┐Óżż ÓżĢÓż░Óż©ÓżŠ ÓżÜÓżŠÓż╣ÓżżÓźć Óż╣ÓźłÓżé, ÓżĄÓż╣ ÓżēÓż”ÓźŹÓż”ÓźćÓżČÓźŹÓż» ÓżģÓż¬ÓźéÓż░ÓźŹÓżŻ Óż╣ÓźĆ Óż░Óż╣ Óż£ÓżŠÓżÅÓżŚÓżŠÓźż
ÓżåÓż¦ÓźüÓż©Óż┐ÓżĢ Óż¬Óż░Óż┐Óż¬ÓźŹÓż░ÓźćÓżĢÓźŹÓżĘÓźŹÓż»- ÓżćÓżĖÓźĆ ÓżżÓżźÓźŹÓż» ÓżĢÓźŗ ÓżĖÓźŹÓż▓ÓźŗÓżĄÓźćÓż©Óż┐Óż»ÓżŠ ÓżĢÓźć 'Óż£ÓźüÓż¼ÓźøÓżŠÓż©ÓżŠ ÓżĄÓż┐ÓżČÓźŹÓżĄÓżĄÓż┐Óż”ÓźŹÓż»ÓżŠÓż▓Óż»' ÓżĢÓźć Óż¬ÓźŹÓż░ÓźŗÓż½ÓźćÓżĖÓż░ 'Óż¤Óż«ÓżŠÓż£ Óż¬ÓźćÓż¤ÓżĢ' Óż©Óźć ÓżŁÓźĆ ÓżģÓż¬Óż©Óźć ÓżČÓźŗÓż¦ Óż«ÓźćÓżé ÓżĖÓż┐Óż”ÓźŹÓż¦ ÓżĢÓż┐Óż»ÓżŠÓźż ÓżĖÓż©ÓźŹ 2012 Óż«ÓźćÓżé Óż¬ÓźŹÓż░ÓżĢÓżŠÓżČÓż┐Óżż Óż░Óż┐ÓżĖÓż░ÓźŹÓżÜ Óż¬ÓźćÓż¬Óż░ Óż«ÓźćÓżé ÓżĄÓźć ÓżĢÓż╣ÓżżÓźć Óż╣ÓźłÓżé, 'Óż¬ÓźŹÓż░ÓżŁÓżŠÓżĄÓźĆ ÓżóÓżéÓżŚ ÓżĖÓźć ÓżĖÓżéÓżĄÓżŠÓż” ÓżĢÓż░Óż©Óźć ÓżĢÓźĆ ÓżĢÓźŹÓżĘÓż«ÓżżÓżŠ ÓżČÓż┐ÓżĢÓźŹÓżĘÓżĢ ÓżĢÓźĆ Óż«ÓźéÓż▓ Óż”ÓżĢÓźŹÓżĘÓżżÓżŠÓżōÓżé Óż«ÓźćÓżé ÓżĖÓźćÓżÅÓżĢ Óż╣ÓźłÓźż ÓżČÓż┐ÓżĢÓźŹÓżĘÓżŠ ÓżĢÓźć ÓżĢÓźŹÓżĘÓźćÓżżÓźŹÓż░ Óż«ÓźćÓżé ÓżČÓż┐ÓżĢÓźŹÓżĘÓżĢ ÓżĢÓżŠ ÓżģÓżÜÓźŹÓżøÓżŠ ÓżĄÓżĢÓźŹÓżżÓżŠ Óż╣ÓźŗÓż©ÓżŠ Óż¼Óż╣ÓźüÓżż Óż«Óż╣ÓżżÓźŹÓżżÓźŹÓżĄÓż¬ÓźéÓż░ÓźŹÓżŻ ÓżŁÓźéÓż«Óż┐ÓżĢÓżŠ ÓżģÓż”ÓżŠ ÓżĢÓż░ÓżżÓżŠ Óż╣ÓźłÓźż
... ÓżåÓż”Óż░ÓźŹÓżČ ÓżåÓżÜÓżŠÓż░ÓźŹÓż»ÓźŗÓżé ÓżĢÓźć ÓżĖÓżŁÓźĆ ÓżŚÓźüÓżŻÓźŗÓżé ÓżĢÓźŗ Óż¬ÓźéÓż░ÓźŹÓżŻÓżżÓżā ÓżĖÓż«ÓżØÓż©Óźć ÓżĢÓźć Óż▓Óż┐ÓżÅ Óż¬ÓźØÓż┐ÓżÅ ÓżĖÓż┐ÓżżÓżéÓż¼Óż░ 2018 Óż«ÓżŠÓż╣ ÓżĢÓźĆ Óż╣Óż┐Óż©ÓźŹÓż”ÓźĆ ÓżģÓż¢ÓżŻÓźŹÓżĪ Óż£ÓźŹÓż×ÓżŠÓż© Óż«ÓżŠÓżĖÓż┐ÓżĢ Óż¬ÓżżÓźŹÓż░Óż┐ÓżĢÓżŠÓźż





